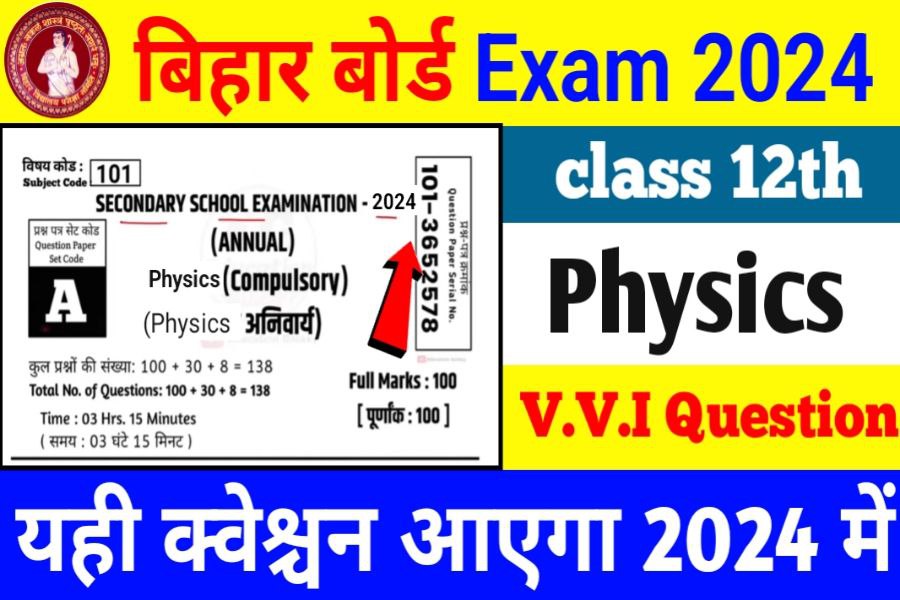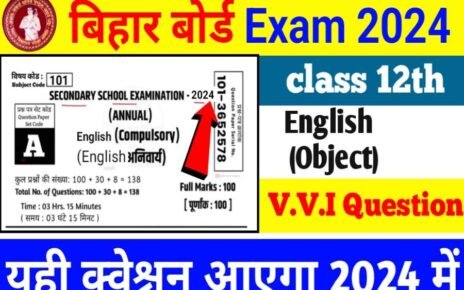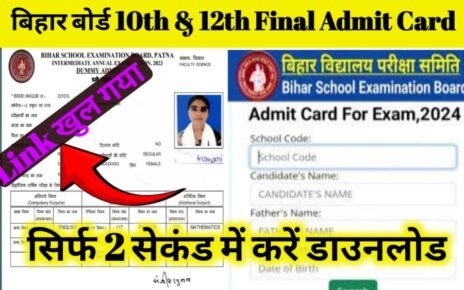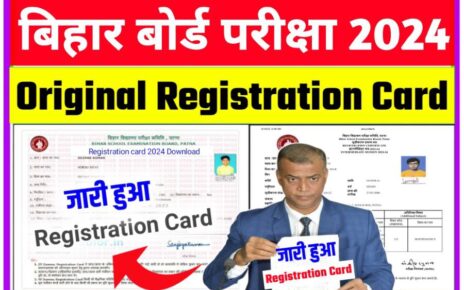Bihar Board 12th Physics Top-15 Question Answer 2024: कक्षा 12वीं परीक्षा 2024 के लिए, Important Physics Top-15 Question Answer 2024
Bihar Board 12th Physics Top-15 Question Answer 2024
प्रश्न 1. प्रतिरोध-बक्स में लगी तार की कुंडलियाँ तार को दोहरा करके क्यों बनाई जाती है?
उत्तर- प्रतिरोध-बक्स में प्रत्येक प्लग के नीचे पीतल के गुटकों से प्रतिरोध-तार की कुंडली संबंधित रहती है। प्रतिरोध-तार को दोहरा करके एक अचालक पदार्थ के छोटे बेलन पर कुंडली के रूप में लपेटा जाता है। दोहरा कर लपेटा प्रतिरोध-तार प्रत्येक स्थान पर एक-दूसरे से विद्युतरोधित (insulated) रहता है। तार को दोहरा कर देने से इससे बनी कुंडली में धारा प्रत्येक स्थान पर दो विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होती है जिस कारण कुंडली से संबद्ध (linked) चुंबकीय फ्लक्स का मान हमेशा शून्य होता है। इससे कुंडली के स्वप्रेरण (self-induction) का प्रभाव शून्य होता है। इस प्रकार, दोहरे तार की बनी कुंडली के रहने से परिपथ में प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होती।
प्रश्न 2. विभवमापी एवं वोल्टमीटर दोनों का व्यवहार विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। एक ही काम के लिए इस प्रकार के दो यंत्रों की आवश्यकता क्यों है? ओं के बीन विभवांतर
उत्तर-वोल्टमीटर से जब किसी परिपथ के दो बिन्दुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है तो इससे भी अल्प-धारा प्रवाहित होती है जिससे मुख्य परिपथ की धारा में कुछ कमी हो जाती है। इसके फलस्वरूप उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कुछ कम हो जाता है। सेल का विद्युत-वाहक बल खुले परिपथ में इसकी प्लेटों के बीच का विभवांतर होता है। सेल के सिरों पर वोल्टमीटर लगा देने पर इससे कुछ धारा प्रवाहित होती है और सेल का कुछ आंतरिक प्रतिरोध होने से यह सेल के विभव को कुछ कम करता है। अतः, वोल्टमीटर द्वारा मापा गया विभवांतर या सेल का विद्युत वाहक बल यथार्थ नहीं होता है। परन्तु,
विभवमापी (potentiometer) की संतुलन-विधि में सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। अतः, विभवमापी विभवांतर या सेल के विद्युत-वाहक बल
का यथार्थ मान देता है। इसके अतिरिक्त चूँकि विभवमापी की विधि शून्य-विक्षेप विधि (null deflection method) है, अतः इससे प्रयोग में विक्षेप-संबंधी
कोई त्रुटि नहीं हो पाती है।
प्रश्न 3. विद्युत द्विध्रुव-आघूर्ण को परिभाषित करें तथा इसका SI मात्रक लिखें।
उत्तर-विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण p कहते हैं। इसका S.I. मात्रक कूलॉम x मीटर होता है।
4. समानांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य है ?
उत्तर–समानांतर प्लेट संधारित्र में दूसरा प्लेट आकार को स्थिर रखते हुए यह पहली प्लेट के विभव को कम कर देती है, अतः उसी विभव पर अधिक आवेश संचित हो जाता है।
प्रश्न 5. शंट के दो उपयोग लिखें।
उत्तर-शंट के दो उपयोग निम्नलिखित हैं-(i) इसके उपयोग से सुग्राही विद्युत् धारामापी या गैल्वेनोमीटर को नुकसान से बचाया जाता है।
(ii) शंट के उपयोग से धारा को विभक्त किया जाता है तथा शंट के मान को बदलकर धारामापी के परास को बढ़ाया जा सकता है।
प्रश्न 6. ऐमीटर में शंट क्यों लगा रहता है?
उत्तर-किसी विद्युत परिपथ से प्रवाहित होनेवाली धारा का मान मापने के लिए ऐमीटर को परिपथ में हमेशा श्रेणीक्रम में जोड़ना चाहिए जिससे कि
कुल धारा ऐमीटर से होकर प्रवाहित हो सके। ऐमीटर का प्रतिरोध कम-से-कम होना चाहिए जिससे कि परिपथ से प्रवाहित धारा का मान न बदले। ऐमीटर का प्रतिरोध न्यूनतम करने के लिए उसके समांतरक्रम में बहुत कम प्रतिरोध का शंट
लगा दिया जाता है क्योंकि जब दो प्रतिरोध S और G (मान लिया) समांतरक्रमGS
में जोड़े जाते हैं तब उनका तुल्य प्रतिरोध R = है, R=GS. होता और इस सूत्र
_
G+S से स्पष्ट है कि R का मान S तथा G दोनों से कम होगा। अतः, शंट S का मान बहुत कम लेकर ऐमीटर के तुल्य प्रतिरोध का मान न्यूनतम किया जा सकता है। एक आदर्श ऐमीटर वह है जिसे परिपथ में लगा देने पर उसमें प्रवाहित धारा
का मान न बदले। यह तभी संभव है जबकि ऐमीटर का प्रतिरोध शून्य हो जाए। चूँकि प्रतिरोध शून्य नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे न्यूनतम किया जाता है।
प्रश्न 7. माडुलन को परिभाषित करें। इसके प्रकारों को लिखें
उत्तर-निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नलों को अधिक दूरियों तक प्रेषित नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रेषित पर, निम्न आवृत्ति के संदेश सिग्नलों को
सूचनाओं को किसी उच्च आवृत्ति की तरंग पर अध्यारोपित (superpose किया जाता है जो सूचना के वाहक (carrier) की भाँति व्यवहार करती है इस प्रक्रिया को मॉडुलन कहते हैं ।
मांडलन तीन प्रकार के होते हैं–(i) आयाम मॉडलन (ii) आवृत्ति मॉडुलन (iii)कला मॉडुलन ।
प्रश्न 8. तप्त तार यंत्र का व्यवहार प्रत्यावर्ती धारा तथा सरल धारा दोनों के मान निकालने में किया जाता है, क्यों?
उत्तर-धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग कर तप्त तार यंत्र अर्थात् तप्त तार ऐमीटर तथा तप्त तार वोल्टमीटर बनाए जाते हैं। इनमें एक तार इस प्रकार व्यवस्थित रहता है कि जब इन यंत्रों से विद्युत-धारा प्रवाहित की जाती है तब तार गर्म होकर लंबाई में बढ़ जाता है जिससे इससे जुड़ा सूचक (pointer) स्केल पर विक्षेपित होकर धारा और विभवांतर का पाठ्यांक देता है। उत्पन
ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती (Woc 2) होती है। इसलिए तार की लंबाई में वृद्धि भी धारा के वर्ग के समानुपाती होती है जिस कारण यह वृद्धि धारा के प्रवाह की दिशा पर निर्भर नहीं करती। प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा एक निश्चित समयांतराल पर बदलती रहती है, परंतु तार में उत्पन्न ऊष्मा धारा के परिमाण पर निर्भर करती है, न कि उसकी दिशा पर। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि तप्त तार ऐमीटर और वोल्टमीटर प्रत्यावर्ती धारा मापने और प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल मापने के लिए व्यवहार में लाए जा सकते हैं। इससे यह भी स्पष्ट है कि तप्त तार यंत्रों (ऐमीटर तथा वोल्टमीटर) का व्यवहार सरल धारा (direct current) मापने के लिए भी किया जा सकता है।
9. किसी ट्रांसफॉर्मर का क्रोड पट्टियों में विभक्त क्या रहता है?अथवा, समझाइए कि ट्रांसफॉर्मर का आंतरक परतदार क्यों होता है?
उत्तर ट्रांसफॉर्मर के लोहे के क्रोड (आंतरिक) में फ्लक्स-परिवर्तन के कारण भँवर-धाराएँ (eddy currents) उत्पन्न हो जाती हैं जिनके कारण लोहे का क्रोड गर्म हो जाता है। इस प्रकार विद्युत-ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में क्षय होता है—इसे लौह क्षय (iron loss) कहा जाता है। इस हानि को कम करने के लिए क्रोड को एक-दूसरी से विद्युतरोधित लोहे की पट्टियों द्वारा परतदार (laminated) बनाया जाता है और क्रोड को परतदार कहा जाता है। ऐसा करने से पट्टियों के बीच उच्च प्रतिरोध होने के कारण उसमें से कोई भँवर-धारा प्रवाहित नहीं होती जिससे लौह क्षय घट जाता है। यही कारण है कि क्रोड को परतदार बनाया जाता है।
प्रश्न 10. दो विद्युत बल रेखाएँ क्यों एक-दूसरे को काट नहीं सकती हैं ? क्या दो समविभव सतह काट सकती हैं ?
उत्तर -यदि दो विद्युत बल रेखाएँ एक-दूसरे को काटती है तो प्रतिच्छेद बिन्दु पर दो स्पर्श रेखाएँ होंगी । इसका अर्थ है कि उस बिन्दु पर विद्युत क्षेत्र के दो मान हैं जो कि संभव नहीं है। नहीं, क्योंकि दो समविभव पृष्ठ प्रतिच्छेदित करते हैं तो प्रतिच्छेद-बिन्दु पर वैद्युत विभव के दो मान होगें जो संभव नहीं है ।
प्रश्न 11. खतरे का चिह्न हमेशा लाल लिया जाता है, क्यों?
उत्तर-रैले नामक एक वैज्ञानिक ने यह प्रतिपादित किया कि सूर्य की किरणों में सभी वर्तमान तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन (scattering) होता है तथा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य 2 के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लाल वर्ण के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है और कि इसके कम प्रकीर्णन के कारण यह काफी दूर से ही दिखाई देता है। यही कारण है कि खतरे का चिह्न हमेशा लाल ही लिया जाता है।
प्रश्न 12. प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष (rainbow) में अंतर स्पष्ट करें।
उत्तर-जब सूर्य का श्वेत प्रकाश वर्षा के समय वर्षा की बूँदों पर पड़ता है तो कभी-कभी, हमें पीठ सूर्य की ओर रखने पर सात रंगोंवाली संकेंद्री चाप दिखाई पड़ती हैं। इन रंगीन चापों को इंद्रधनुष कहते हैं। बहुधा दो इंद्रधनुष एक साथ दिखाई पड़ते हैं, जो एक-दूसरे के ऊपर रहते हैं। अंदरवाले इंद्रधनुष को प्राथमिक इंद्रधनुष तथा बाहरवाले को द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। दोनों ही प्रकार के इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण-विक्षेपण (dispersion) के कारण दिखाई देते हैं।
प्राथमिक इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश के उन किरणों द्वारा दिखाई देता है जिनका वर्षा की बूँदों के अंदर दो बार अपवर्तन और एक बार आंतरिक परावर्तन के बाद न्यूनतम विचलन होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश के उन किरणों से दिखाई देता है जिनका वर्षा की बूँदों में दो बार अपवर्तन तथा दो बार आंतरिक परावर्तन के बाद न्यूनतम विचलन होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष की अपेक्षा प्राथमिक इंद्रधनुष अधिक चमकीला और छोटा होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष का भीतरी कोर बैंगनी (violet) और बाहरी कोर लाल (red) होता है। इसके ठीक विपरीत द्वितीयक इंद्रधनुष में होता है, अर्थात् इसका भीतरी कोर लाल और बाहरी कोर बैंगनी होता है। चूँकि द्वितीयक इंद्रधनुष बनानेवाली किरणों की तीव्रता दो बार आंतरिक परावर्तन के कारण कम हो जाती है, इसीलिए यह इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में कम चमकीला होता है।
प्रश्न 13. विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लेंज नियम लिखें ।
उत्तर-लेंज के नियम से विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित विद्युत् वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा से ज्ञात की जाती है । इस नियम के अनुसार, “विद्युत् चुंबकीय प्रेरण के कारण सभी अवस्थाओं में किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का हो विरोध करती हैं जिसके कारण प्रेरित धारा स्वयं उत्पन्न होती है ।
प्रश्न14. ट्रांसफॉर्मर का क्रोड परतदार क्यों होता है ?
उत्तर-ट्रांसफॉर्मर का क्रोड परतदार होता है क्योंकि क्रोड में लौह-क्षय होता है। भँवर धाराओं के प्रेरित होने से ट्रांसफॉर्मर के क्रोड में विद्युत शक्ति की हानि होती है। जिसे लौह-क्षय कहा जाता है। क्रोड को परतदार होने से लौह-क्षय का मान कम हो जाता है। इसलिए क्रोड परतदार होता है ।
प्रश्न 15. तापायनिक उत्सर्जन की प्रक्रिया सिर्फ सतह पर क्यों घटती है ?
उत्तर- प्रकाश उत्सर्जन की घटना सिर्फ धातु सतह पर ही घटती क्योंकि धातुओं के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि ऊष्मा पाकर सतह से बाहर निकलते हैं।